कुछ समय पहले तक जिन विषयों पर बात करना फिल्मों के पर्दे पर वर्जित समझा जाता था आज हमारी फिल्में गाहे-बगाहे उन पर खुल कर कह-बोल रही हैं. बड़ी बात यह भी है कि ऐसी लीक से हट कर कही जाने वाली कहानियों में दर्शक भी रूचि दिखा रहे हैं बशर्ते कि वे कायदे से बुनी हों और सलीके से बनी हों.
भोपाल में रहने वाला डॉक्टर उदय एम.बी.बी.एस. के बाद हड्डियों का डॉक्टर बनना है लेकिन उसे सीट मिलती है स्त्री रोग की क्लास में. अब एक पुरुष कैसे करे उस ‘चीज’ का इलाज, जो उसके पास है ही नहीं…!
फिल्म वालों ने ऐसी कहानियों को हास्य के रैपर में लपेट कर कहने का जो तरीका निकाला है, यह फिल्म भी उससे परे नहीं है. लेकिन हंसी-ठठ्ठे में यह काफी कुछ गंभीर, काफी कुछ सार्थक कह जाती है. सबसे पहले तो यह फिल्म इस शिकायत को दूर करती है कि हिन्दी वालों के पास कहने को अलग किस्म की कहानियां नहीं हैं. सौरभ भारत और विशाल वाघ की सोची कहानी में नएपन के साथ-साथ दुस्साहस भी भरपूर है. बे-मन से स्त्री रोग की पढ़ाई कर रहे एक पुरुष डॉक्टर की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती कहानी को एक बेहतर पटकथा में तब्दील करने का काम इन दोनों के साथ डायरेक्टर अनुभूति कश्यप ने भी बखूबी किया है. और जब चीजें कागज पर बेहतर बन जाएं तो यह आधी जंग जीतने जैसा होता है.
बाकी की जंग डायरेक्टर अनुभूति ने कैमरे के सामने जीती है. महज़ दो घंटे की लंबाई वाली यह फिल्म भूमिका बांधने, कहानी बताने, किरदारों का परिचय कराने जैसे पचड़ों में पड़े बिना पहले ही सीन से पटरी पर दिखती है और उसके बाद सरपट दौड़े चली जाती है. हालांकि इसकी रफ्तार कहीं-कहीं धीमी पड़ती है और इसमें थोड़ी लचक भी आती है लेकिन दर्शकों का इससे जुड़ाव कम नहीं होता.
दरअसल इस फिल्म में मुख्य कहानी से इतर जो छोटे-छोटे घेरे बनाए गए हैं, दर्शक उनमें भी जा उलझता है. सुमित सक्सेना के संवादों का जिक्र भी जरूरी है जो बिना किसी फूहड़ता के, बिना उपदेशात्मक हुए अपनी बात भी कह जाते हैं और उस बात का असर भी छोड़ जाते हैं. सच यह भी है कि इस फिल्म के संवाद सचमुच ‘सुनने’ लायक हैं जो असर भी छोड़ते हैं.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
अभी सब्सक्राइब करें
असल में इस किस्म के विषयों के साथ सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी होती है कि बात कहीं अश्लील न हो जाए और कहीं उपदेश न पिलाने लगे. ‘बधाई हो’ सरीखा पैनापन इस किस्म के विषयों वाली फिल्मों में कम ही दिखा है. यह फिल्म भी ‘बधाई हो’ के स्तर को भले ही न छू पाई हो, उसके आसपास तो पहुंची ही है. फिल्म की एक बड़ी खूबी यह भी है कि यह न तो डॉक्टरी की भाषा में कहीं फिसली है और न ही भोपाल की बोली में. इन दोनों ही कामों के लिए दो विशेषज्ञों को रखने से यह सुखद नतीजा आया है. हां, क्लाइमैक्स को थोड़ा और कसा जाता तो यह मारक हो सकती थी.
आयुष्मान खुराना इस किस्म के किरदारों में बंध भले ही गए हों, लेकिन वह बुरे बिल्कुल नहीं लगते हैं. रकुल प्रीत सिंह को इस फिल्म में देखना सुखद अहसास देता है. शेफाली शाह और शीबा चड्ढा तो जैसे हद दर्जे का उम्दा अभिनय करने की कसम खाकर कैमरे के सामने आती हैं. काम बाकी कलाकारों-परेश पाहूजा, अभय चिंतामणि, अंजू गौड़, झुम्मा मित्रा आदि का भी अच्छा है लेकिन कहीं-कहीं महसूस होता है कि इनमें से कुछ किरदारों को और विस्तार दिया जाना चाहिए था.
वास्तविक लोकेशनों पर शूट किया जाना फिल्म को बल देता है. गीत-संगीत कहानी के प्रवाह में घुल-मिल जाते हैं. ‘ए’ सर्टिफिकेट होने के कारण बच्चों के मतलब की फिल्म नहीं है यह. उम्दा मनोरंजन और बढ़िया कहानी देखनी हो तो तुरंत मिलें इस डॉक्टर जी से.

(दीपक दुआ 1993 से फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं. विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए सिनेमा व पर्यटन पर नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
श्रेय: स्रोत लिंक
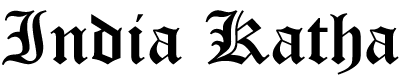









इस बारे में चर्चा post