विनोद अनुपम।
‘अब कोर्ट में खुलेगी कामेडी की दुकान’, इस टैगलाइन के साथ कुछ दिनों पहले ‘अमेजन मिनी टीवी’ ने एक नए कामेडी शो की शुरुआत की थी। सच तो यही है कि हिंदी सिनेमा, टेलीविजन और फिर वेब सीरीज में कमोबेश अदालतों का उपयोग वास्तविकता से परे मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होता आया है। यह भी एक सत्य है कि देश में आमतौर पर लोग अदालतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा कि अधिकांश के जीवन में अदालतों को देखने के अवसर तक नहीं आते। ऐसे में सिनेमा के पास सहूलियत होती है कि वे अपनी कल्पना से एक अदालत गढ़ लें, जिसे दर्शक स्वीकार कर लेंगे। यह कम कमाल की बात नहीं कि सिनेमा में अदालत का सबसे अधिक चर्चित दृश्य, जिसमें गवाह लाल कपड़े में लिपटी एक किताब पर हाथ रख कहते हुए दिखता है, ‘मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा’, का वास्तविकता से कोई सरोकार ही नहीं। देश में अदालत में धार्मिक पुस्तकों की कसम खाने की यह परंपरा 1969 में ही समाप्त हो गई थी और उसके स्थान पर ‘ओथ एक्ट, 1969’ पास किया गया, जिसके अनुसार अब शपथ एक, सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर दिलाई जाती है। यहां पर यह भी गौरतलब है कि कि ओथ एक्ट, 1969 के अनुसार 12 साल से कम उम्र के गवाह को किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होती क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं।
खत्म हुई जूरी की मंजूरी
यहां 2016 में आई ‘रुस्तम’ और 1986 की फिल्म ‘एक रुका हुआ फैसला’ का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें अदालतों में जज के साथ जूरी भी दिखाई गई थी। ‘रुस्तम’ 2016 की सबसे बड़ी हिट हुई और इस फिल्म में अभिनय के लिए अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। ‘रुस्तम’ एक सत्य घटना पर आधारित थी, कहते हैं बीसवीं सदी के नौंवे दशक में पहली बार मीडिया और जनसमूह ने किसी फैसले को प्रभावित किया था, लेकिन बाद में न्यायालय ने न सिर्फ जूरी के निर्णय को ही पलट दिया, बल्कि न्यायप्रक्रिया में जूरी की समाप्ति की भी अनुशंसा कर दी। अब यह प्रक्रिया सिर्फ पीरियड फिल्मों में ही देखी जा सकती है।
वास्तविकता दिखाने का गंभीर प्रयास
वास्तव में सिनेमा में अदालतों का उपयोग पहले ‘आवारा’ जैसी फिल्म में दर्शकों की भावनाओं को कुरेदने के लिए किया जाता था, फिर सस्पेंस के लिए किया जाने लगा। वेब सीरीजों में तो वकील, वकील से ज्यादा जासूस की भूमिका में दिखने लगे। हालांकि बी. आर. चोपड़ा ने 1960 में ‘कानून’ में अदालत को पूरी निष्ठा के साथ दिखाने की शुरुआत की थी। उस दौर में गानों की लोकप्रियता से ही फिल्में हिट हुआ करती थीं, लेकिन चोपड़ा साहब ने विषय की गंभीरता को देखते हुए हिंदी में पहली बार बगैर गानों की फिल्म बनाने की हिम्मत जुटाई। कहते हैं इस फिल्म की चुनौती को देखते हुए अशोक कुमार ने बगैर अपनी फीस के काम कर उन्हें सहयोग दिया था। चोपड़ा साहब सिनेमा के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के लिए जाने जाते थे, यह फिल्म भी उस दौर में फांसी की सजा पर बात करती थी, लेकिन यही बी. आर. चोपड़ा 1980 में जब दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ‘इंसाफ का तराजू’ लाते हैं, तब न तो अदालतों की प्रस्तुति में सच्चाई दिखती है, न ही बहसों में गंभीरता।
असली न्यायालय तक पहुंची बात
दुष्कर्म के मुद्दे पर अदालती प्रक्रिया तो बाद में कई फिल्मों में दिखी, लेकिन अधिकांश का उद्देश्य दर्शकों को मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाने के बजाए मनोरंजित करने की ही रही। ऐसे में ‘दामिनी’ जरूर अलग दिखती है जिसमें एक बहू किसी महिला के सम्मान के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसे साथ मिलता है एक सामान्य वकील का। इस फिल्म में सनी देओल के संवाद ‘तारीख पर तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता’ की प्रासंगिकता इसी से समझी जा सकती है कि हाल ही में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी इसी संवाद के साथ वकीलों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
मिलती हैं बस तालियां
वहीं 2019 में जब ‘सेक्शन 375’ आती है तो लगता है, समय के साथ समाज कितना बदल चुका है। अक्षय खन्ना अभिनीत यह फिल्म दुष्कर्म के झूठे मुकदमों के बढ़ते प्रचलन पर पूरी गंभीरता से सवाल उठाती है। यहां 2004 में आई अब्बास मस्तान की ‘ऐतराज’ का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पत्नी अदालत में अपने पति पर दुष्कर्म के लगाए झूठे मुकदमे के खिलाफ लड़ती है। हाल के दिनों में जब सिनेमा में कहानी की मांग बढ़ी, तो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाती ‘जाली एलएलबी’ की तरह कई फिल्में आईं। ‘नो वन किल्ड जेसिका’ और ‘तलवार’ जैसी बहुचर्चित घटनाओं पर न्यायालयों की सीमा रेखांकित करती महत्वपूर्ण फिल्में भी आईं। ‘पिंक’ ने अदालती कार्यवाही के बहाने महिला अधिकार के मुद्दे पर सार्थक संवाद की कोशिश की। वास्तव में अदालती दृश्यों में संवादों का महत्व इसी बात पर है कि वे न्यायिक प्रक्रिया को किस तरह स्पष्ट करते हैं, लेकिन आमतौर पर अदालती दृश्यों में संवाद बस दर्शकों की तालियों को ही ध्यान में रख लिखे जाते हैं। सुभाष घई की ‘मेरी जंग’, टी. रामाराव की ‘अंधा कानून’ जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें अदालतें तो दिखती हैं, लेकिन देश की न्याय प्रक्रिया से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ‘वीर जारा’ में वीर यानी शाह रुख खान की पाकिस्तान कोर्ट में पढ़ी वह कविता याद कीजिए…‘मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूं/इस मिट्टी से मेरे बाउ जी के खेतों की खुशबू आती है/वो कहते हैं ये तेरा देस नहीं/फिर क्यों मेरे देस जैसा लगता है..’ तो कोर्ट हमने ऐसा भी देखा है, बड़े परदे पर।
वेब सीरीज उसी राह पर
हालांकि यह सवाल अपनी जगह है कि ‘मी लार्ड’, ‘मेरे काबिल दोस्त’, ‘बाइज्जत बरी’ की फिल्मी अदालतों की इस दुनिया का हमारे न्यायिक मामलों और लोगों की भीड़ से अटी पड़ी अदालतों से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मुश्किल यह कि अदालतों के प्रति सिनेमा की बनाई धारणा को वेब सीरीज भी चुनौती देने की कोशिश करते नहीं लगते हैं। हिंदी की वेब सीरीज ने लोकप्रियता के लिए अपराध, हत्या, दुष्कर्म जैसी कहानियों का आसान रास्ता चुना है। जाहिर है, फिल्मी अदालतें उनकी राह आसान बना देती हैं। ‘क्रिमिनल जस्टिस’, ‘योर आनर’, ‘गिल्टी माइंड्स’, ‘इलीगल-जस्टिस, आउट आफ आर्डर’ जैसी सीरीज मूलत: अपराध कथा के लिए ही याद रहती हैं, न्यायिक प्रक्रिया के लिए नहीं। लगता है पटकथा यह तय ही नहीं कर पाती कि वकील को वकील रखा जाए या फिर इन्वेस्टिंग अफसर या प्राइवेट जासूस। जो भी हो, जैसे भी हो, फिल्में और वेब सीरीज न्यायिक प्रक्रिया पर जब तक हमारा भरोसा बनाए रखती हैं, हम इन कहानियों से आनंदित तो हो ही सकते हैं। बस, इससे उत्साहित होकर कोई निर्माता न्यायालय को कामेडी की दुकान न बना दे।
Edited By: Aarti Tiwari
श्रेय: स्रोत लिंक
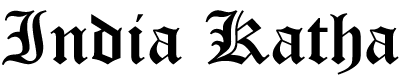









इस बारे में चर्चा post